- January 21, 2021
मातृभाषा और बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं का महत्व—राहुल देव
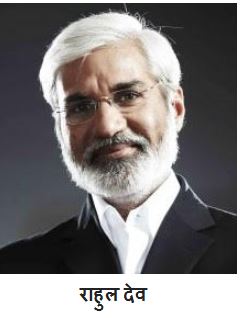
किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी मातृभाषा के महत्व की सबसे अच्छी और सटीक तुलना करने के लिए माँ के दूध से बेहतर कुछ नहीं। जैसे जन्म के एक या दो वर्ष तक बच्चे के शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए माँ का दूध और स्पर्श सर्वश्रेष्ठ होते हैं वैसे ही उसके संवेगात्मक, बौद्धिक और भाषिक विकास के लिए मातृभाषा या माँ बोली। मातृभाषा की इस भूमिका पर संसार में कोई भी मतभेद नहीं है, वैसे ही जैसे माँ के दूध के महत्व, प्रभाव और भूमिका पर कोई मतभिन्नता नहीं है।
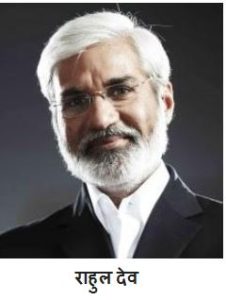
बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा में मातृभाषा या पारिवारिक भाषा या परिवेश/स्थानीय भाषा का महत्व उन मुट्ठी भर विषयों में है जिस पर पूरी दुनिया के शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों की सर्वानुमति है। इस विषय पर इतने सारे शोध, प्रयोग, अध्ययन हुए हैं, इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं कि अब इसे एक सार्वभौमिक निर्विवाद सत्य के रूप में वैश्विक स्वीकृति मिल गई है। शिक्षाविद् जानते हैं कि 6 साल की उम्र तक बच्चों के ८०-८५ प्रतिशत मस्तिष्क का विकास हो जाता है। यह भी अब एक सर्वविदित तथ्य है कि दो से आठ साल की उम्र के बीच कई भाषाएं आसानी से सीख लेने की क्षमता बच्चों में सबसे प्रबल होती है।
शोधों ने यह सिद्ध किया है कि जीवन के आरंभिक वर्षों और प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों में सर्वश्रेष्ठ संवेगात्मक विकास के साथ साथ सभी विषयों की समझ और अधिगम भी बेहतर होते हैं उन बच्चों की तुलना में जिन्हें अपनी मातृभाषा/परिवेश भाषा से अलकिसी भाषा में पढ़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, दूसरी भाषाएं सीखने में भी मातृभाषा/परिवेश भाषा में पढ़ने वाले बच्चे आगे पाए गए उन दूसरी श्रेणी के बच्चों की तुलना में। यानी प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा माध्यम शिक्षा बच्चों को बहुभाषी बनाने में भी श्रेष्ठतर साबित होती है।
यह तथ्य अकेला ही पर्याप्त है यह सिद्ध करने के लिए कि दुनिया के किसी भी स्थान-समाज में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए मातृभाषा/परिवेश/स्थानीय भाषा ही सर्वांगीण विकास तथा सभी विषयों के बारे में सीखने के लिए सर्वोत्तम माध्यम होती है। यह बात सुदूर जंगलों में रहने वाले वनवासी बच्चों पर भी उतनी है लागू होती है जितनी सबसे विकसित, संपन्न समाजों-देशों के बच्चों पर।
यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषाविदों के अनुसार समाज विकसित या अविकसित हो सकते हैं लेकिन कोई भी भाषा अविकसित नहीं होती। संसार की हर भाषा में अपने बोलने-बरतने वालों की सभी संचार-अभिव्यक्ति-आवश्यकताओं को पूरा करने की अन्तर्निहित क्षमता होती है।
यह बात इसलिए केन्द्रीय महत्व की है कि बहुत से ऐसे देशों-समाजों में जो आधुनिक विकास, संपन्नता, तकनीकी-आर्थिक प्रगति में विकसित देशों से पिछड़ गए हैं, लोगों के मन में यह बात बिठा दी जाती है कि उनकी अपनी देशज, स्थानीय भाषाएं विकसित देशों की तथाकथित विकसित भाषाओं की तुलना में अविकसित, गरीब और असमृद्ध हैं। यह स्थिति ज्यादातर उन देशों की है जो किसी न किसी औपनिवेशिक देश की दासता के शिकार रहे हैं। अपनी भाषा-संस्कृति-समाज-समझ की हीनता का यह भाव इन समाजों में अपनी विरासत, अपनी हर बात को लेकर एक गहरा हीनता-भाव, आत्म-लज्जा भर देता है। उनके आत्म-विश्वास को खंडित कर देता है।
इस औपनिवेशिकता-जनित आत्महीनता का एक परिणाम यह होता है कि ऐसे विजित समाज अपनी भाषा, अपनी सांस्कृतिक पहचान, तौर-तरीकों, परंपराओं, पद्धतियों, ज्ञान-परंपराओं को लेकर गहरे संशय और अविश्वास से भर जाते हैं। उन्हें विजेता समाज, संस्कृति, भाषा, शिक्षा, जीवन शैली श्रेष्ठतर लगने लगते हैं। परिणामतः वे अपने पारंपरिक तौर तरीके छोड़ कर विजेता या प्रभुत्वशाली वर्ग के तौर तरीके अपनाने लगते हैं। उनकी नकल करने लगते हैं। विश्व के सभी पूर्व-औपनिवेशित देश-समाज इस आत्महंता चेतना से ग्रस्त हो गहरी और व्यापक सांस्कृतिक-बौद्धिक-शैक्षिक दासता के शिकार बने दिखते हैं भले ही उन्हें राजनीतिक स्वाधीनता मिल गई हो।
सांस्कृतिक दासता का एक स्पष्ट परिणाम उस समाज में नवाचार, मौलिक चिंतन, शोध, आविष्कारों की कमी में दिखता है। चूँकि समाज का शिक्षित वर्ग पराई शिक्षा पद्धति और विचार सरणियों की नकल करना ह्रदयंगम कर चुका होता है इसलिए अपनी नैसर्गिक प्रकृति तथा प्रतिभा की नींव पर मौलिक विचार, कल्पनाओं और नवोन्मेष की उसकी क्षमता क्षीण पड़ जाती है।
भाषायी साम्राज्यवाद- “वह परिघटना जिसमें एक भाषा के बोलने वालों के मन-मस्तिष्क और जीवन एक दूसरी भाषा द्वारा इतने दबा दिए जाते हैं कि वे यह विश्वास करते हैं कि जब मामला जीवन के उच्चरतर पहलुओं का हो तो वे उसी विदेशी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए जब मामला जीवन के उन्नत पक्षों से, जैसे शिक्षा, दर्शन, साहित्य, शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था आदि, निपटने का हो। भाषायी साम्राज्यवाद में किसी समाज के श्रेष्ठ लोगों के भी मानस, दृष्टिकोणों और आकांक्षाओं को विकृत करने और उन्हें देशज भाषाणों के सही मूल्यांकन तथा उनकी संपूर्ण संभावनाओं का अहसास करने से रोकने की एक शक्ति है।“
(ऐन्स्रे, १९७९)
भारत भी इस ऐतिहासिक विकार, भाषायी साम्राज्यवाद का शिकार है।
इस विषय का दूसरा पहलू बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा या भाषा की भूमिका का है। इसे समझने से पहले यह जरूरी है कि भाषा के बारे में इस सबसे बड़ी लगभग वैश्विक और सार्वभौमिक गलतफहमी को दूर किया जाए कि भाषा केवल संवाद का माध्यम है। जब तक इस भ्रम को दूर नहीं किया जाता और भाषा की ज्यादा बड़ी भूमिका को ठीक से नहीं समझा जाता तब तक बच्चों की प्रारंभिक देखभाल तथा शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को नहीं समझा जा सकता। जिस तरह गर्भनाल के माध्यम से बच्चे को मां के गर्भ में सारा पोषण प्राप्त होता है, धीरे-धीरे उसके विभिन्न अंगों और पूरे शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही बच्चे की माँ/परिवार/परिवेश की भाषा उसके अंतःशरीर या अंतःकरण के गठन में निभाती है।
दृष्टि, स्पर्श, ध्वनियां और स्वाद- मुख्यतः जन्म के समय से सक्रिय इन चार इंद्रियों के माध्यम से भीतर जाने वाले अनुभवों, अनुभूतियों, प्रभावों से बच्चे की आंतरिक दुनिया बनती है। बच्चा जो देखता है, जिन्हें देखता है, जिन ध्वनियों को सुनता है, जिन स्पर्शों को महसूस करता है उनके दैनिक अनुभव से धीरे-धीरे उस की चेतना को कोरे पन्ने पर अनुभवों का कोश बढ़ता जाता है और बाहरी संसार के इन अनुभवों से, परिचित-सुखद अनुभूतियाँ देने वाले चेहरों-आवाज़ों-स्पर्शों से उसके रिश्तों और ज्ञान का आंतरिक संसार बनता जाता है।
यही आंतरिक संसार धीरे-धीरे बच्चे के आत्मबोध में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका परिचय अपने परिवार से शुरू होकर अपने परिवेश से होने लगता है। शैशव के इस बीजरूपी आत्मबोध से वयस्क होने पर संसार-बोध तक की इस यात्रा में उसकी इन्द्रियां ही सबसे अधिक सहायक होती है। इन ऐन्द्रिक अनुभवों के माध्यम से वह जानता और पहचानता है माँ को, पिता को, निकट परिजनों को, घर को, विविध रूपों और वस्तुओं को, विभिन्न ध्वनियों और उनके स्रोतों-आशयों-अर्थों को। और रूपाकारों, पारिवारिक तथा पारिवेशिक व्यक्तियों, संबंधों और वस्तुओं, नामों, उनके अर्थों तथा प्रयोजनों से उसका ज्ञान संसार भरता जाता है।
और जैसे-जैसे यह संसार बड़ा होता जाता है, बच्चा इसके अनुभवों को ह्रदयंगम करता जाता है। वह सहज मानवीय प्रतिक्रिया में अपने इस अंतरंग संसार से संवाद करना शुरू कर देता है, हाथ-पैर चला कर, मुखमुद्राओं से, किलकारियों या रुदन से, फिर अपनी तोतली अनगढ़ बातों से अपने को व्यक्त करना शुरू कर देता है। तब तक प्रमुखतः माँ और दूसरे परिजनों को सुनते-सुनते ध्वनियों, शब्दों, अर्थों, आशयों का उसका कोश भी बढ़ते हुए तुतुलाने से शुरू होकर एक दिन माँ/मम्मा शब्द से भाषा में बदल जाता है। यहाँ से बच्चे का भाषा भंडार आश्चर्चजनक तेजी से भरने लगता है। ये डेढ़-दो साल से आठ साल बच्चों के भाषिक, संवेगात्मक विकास के सबसे उत्कट साल होते हैं। ये अपने घर से आरंभ करके बाहर के वृहत्तर संसार से रोज़ सघन और विविधतापूर्ण परिचय के वे वर्ष हैं जब बच्चा सोख्ते की तरह हर चीज़ ग्रहण करता है। ये ही वे वर्ष हैं जब उसकी शाला-पूर्व शिक्षा आरंभ होती है और कक्षा आठ तक चलती है।
इस भाषा से ही बच्चा अपने रोज बढ़ते, विस्तृत होते संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, उससे संबंध स्थापित करता है। ये संबंध केवल बौद्धिक जानकारी के ही नहीं स्थानीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक तथा संवेगात्मक भी होते हैं। अपने भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक ज्ञान तथा सहज जिज्ञासा से बच्चा अवचेतन स्तर पर ही संसार की खोज करता जाता है और इस तरह अपने आपको उसमें स्थापित भी करता जाता है।
इस प्रारंभिक भूमिका के बाद जब हम भारतीय शैक्षिक परिदृश्य को देखते हैं तो पाते हैं कि ७२ साल की स्वाधीनता के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था की ध्वस्त अवस्था, हमारी भाषाओं की बढ़ती अप्रासंगिकता, हमारे करोड़ों शिक्षित युवाओं की रोजगार-अयोग्यता, देश में नवाचार और मौलिक वैज्ञानिक आविष्कारों की लज्जाजनक कमी, आधुनिक ज्ञान के विविध क्षेत्रों में विश्वस्तरीय मौलिक चिंतन, पुस्तकों, खोजों का अभाव, आर्थिक-सामाजिक पिछड़ापन जैसी बातें सामने खड़ी दिखती हैं।
इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार कारणों, वर्गों में प्रमुख हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नेतृत्व है जिसने स्वाधीनता के बाद भी भारत की बौ्द्धक आजादी की नींव यानी शैक्षिक आजादी के महत्व को नहीं समझा और शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी, आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किए। अंग्रेजों द्वारा अपने औपनिवेशिक हितों के लिए बनाया गया शिक्षा तंत्र ही मामूली बदलावों के साथ जारी रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अस्थिर स्थितियों और चुनौतियों से जूझते राजनीतिक-शैक्षिक नेतृत्व ने कुछ इस दबाव में और कुछ बौद्धिक आलस्य में शिक्षा की वह सुविचारित नई प्रणाली विकसित नहीं की जो भारत की प्रकृति, परंपरा और प्रतिभा के अनुरूप इस नए भारत के स्वप्न को मूर्त रूप दे पाती। इस बौद्धिक आलस्य में राजभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी जारी रख कर उसके प्रभुत्व, प्रभाव को बनाए रखना भी था और शिक्षा की माध्यम भाषा के रूप में बनाए रखना भी, विशेषतः उच्चतर शिक्षा में।शासन, उद्योग, ज्ञान-विज्ञान में अंग्रेजी का प्रभाव, शक्ति और प्रतिष्ठा घटे नहीं, बढ़ते रहे। इनका स्वाभाविक असर प्राथमिक शिक्षा पर पड़ा और धीरे-धीरे उसमें भी स्थानीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी ही माध्यम भाषा के रुप में बढ़ती रही। इस विदेशी भाषा से मिलने वाले प्रगति और रोजगार के अवसरों, सामाजिक प्रतिष्ठा के आकर्षण में अभिभावको की कई पीढ़ियों ने अपने बच्चों को भाषाई माध्यम की जगह अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भर्ती कराया। इस तरह इन बच्चों के साथ ऐसी अनेक पीढ़ियाँ तैयार हो गईं जो बचपन से ही अपनी-अपनी भाषाओं से शिक्षा, ज्ञान ग्रहण तथा गंभीर अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में दूर हो चुकी थीं। वे अपनी भाषाओं का बातचीत, जीवन के सामान्य व्यापार में तो इस्तेमाल करती थीं लेकिन जीवन के ज्यादा महत्वपूर्ण आयामों में अंग्रेजी पर ही निर्भर थी, उसकी अभ्यस्त बना दी गई थीं।
इसका परिणाम आज इस रूप में हमारे सामने है कि एक ओर तो गरीब से गरीब अभिभावक भी अपने बच्चों को अच्छे भाषा-माध्यम सरकारी विद्यालयों से हटा कर तथाकथित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में डाल रहे हैं भले ही वे कितने भी घटिया और मँहगे हों। दूसरी ओर, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ कर निकले हमारे दोहरा नुकसान उठा रहे हैं। एक तो उन्हें इस थोपे हुए अंग्रेजी माध्यम के कारण सच्चा विषय-ज्ञान नहीं मिलता, उनका अधिग उथला और अनुपयोगी रहता है। इससे वे शिक्षित डिग्रीधारी तो बन जाते हैं लेकिन ये डिग्रियाँ उनमें रोजगार, अच्छी नौकरियों के लिए सुयोग्य नहीं बनातीं।
दूसरा इससे भी बड़ा नुकसान यह होता है कि वे अपनी भाषाओं की समृद्धि, क्षमताओं, शक्ति और सौन्दर्य से क्रमशः दूर, कटे हुए और अपरिचित होते जाते हैं। चूँकि हमारी सांस्कृतिक पहचान, आत्म-संस्कृति बोध अविच्छिन्न रूप से हमारी विविध भाषाओं से जुड़ा हुआ है, उनके सघन परिचय-प्रयोग से ही विकसित होता है इसलिए ये शिक्षित युवा आत्म विकास के रोजगारपरक रास्तों से तो दूर रहते ही हैं अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपना अस्मिता बोध भी खो देते हैं।
अपनी सांस्कृतिक विरासत, जड़ों, ज्ञान-परंपराओं, अस्मिता के सभ्यतामूलक सूत्रों से यह कटाव प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से पाने वाले बच्चों में भी देखा जा सकता है। इनके साथ ही इन बच्चों के मन में अंग्रेजी-जनित एक अहंकार, भाषा-माध्यम समवय्स्कों, व्यक्तियों के बरक्स एक श्रेष्ठता ग्रंथि भी विकसित हो जाती है। यूँ भारत और इंडिया एक देश के दो नाम ही नहीं दो अलग-अलग मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संसार भी बन गए हैं।
अपनी भाषा बोलने के लिए एक बच्चे को सज़ा देना उस भाषा के विनाश का आरंभ है।“ (भाषाई अधिकारों पर विश्व सम्मेलन, बारसेलोना में बोलते हुए बेनिन के एक प्रतिनिधि, जून 1996)
भारत के हजारों अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में यह शर्मनाक व्यवहार आज भी आम है। इस तरह भारत के विद्यालयों में ही भारत की भाषाओं के विनाश की नींव तैयार की जा रही है।
भारतीय मानस पर अंग्रेजी और अंग्रेजियत के इस प्रभाव ने आम शिक्षित भारतीय को पश्चिमपरस्त, पश्चिमी सभ्यता, ज्ञान-विज्ञान, तकनीक तथा चिंतन का मुखापेक्षी बना कर देश को एक नकलची राष्ट्र बना दिया है। पराई भाषा में मौलिक चिंतन नहीं हो सकता। वह अपनी भाषा में ही संभव है। लेकिन अंग्रेजी के वर्चस्व ने सारी भारतीय भाषाओं को बोलने वालों, उनके परिवेश, परंपराओं, जीवनशैलियों को इस आधुनिक अंग्रेजी-परस्त युवा के लिए पिछड़ा हुआ, अनाधुनिक और शर्म का कारण बना दिया है। इसी कारण भारत में ज्ञान-विज्ञान के उच्चतर क्षेत्रों में नवाचार, मौलिक चितन, शोध, आविष्कार इतने कम हैं।
भारत को यदि इस ज्ञान युग में आधुनिक, प्रगतिशील, समृद्ध और ज्ञान-विज्ञान में अग्रणी बनना है तो उसे अंग्रेजी का यह मूर्खतापूर्ण मोह छोड़ कर अपनी ९०% प्रतिभाओं को उनकी अपनी भाषाओं में शाला-पूर्व स्तर से ही उत्कृष्टतम शिक्षा देकर उनकी मौलिकता तथा रचनाशीलता को उच्चतम प्रस्फुटन के अवसर देने होंगे। अपनी-अपनी मातृ/परिवेश/प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा-संस्कार तथा स्वस्थ आत्म-बोध प्राप्त करके ही ये नई पीढियाँ भारतीय नवोन्मेष का नया युग निर्मित कर सकेंगी।
सौभाग्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दशकों बाद भारतीय राष्ट्र के नवनिर्माण में भारतीय भाषाओं की इस अनिवार्य भूमिका को पहचाना है और प्राथमिक से लेकर उच्चतम स्तर की शिक्षा में उनको केन्द्रीय स्थान दिया है। अगले १५-२० वर्षों में इस नई शिक्षा व्यवस्था से आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, तकनीक तथा एक पुनर्प्राप्त सांस्कृतिक गर्ब और सभ्यता-बोध से संपन्न होकर जह भावी भारतीय संसार में पदार्पण करेंगे तब भारत की वास्तविक प्रतिभा का चमत्कार संसार देखेगा।
इसका प्राथमिक माध्यम बनेंगी भारतीय भाषाएं।
राहुल देव
२७ नवंबर, २०२०




